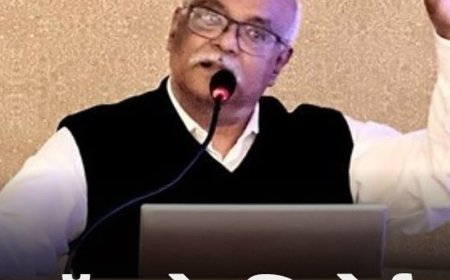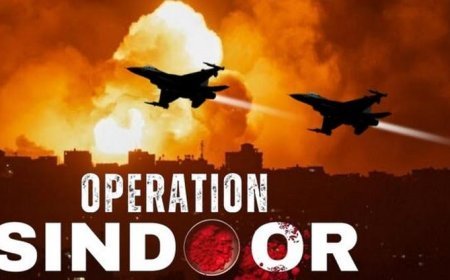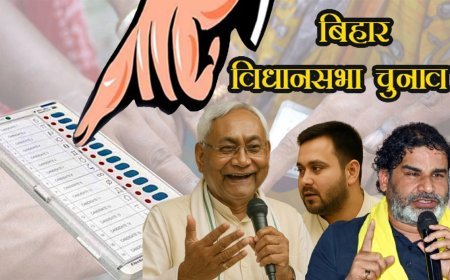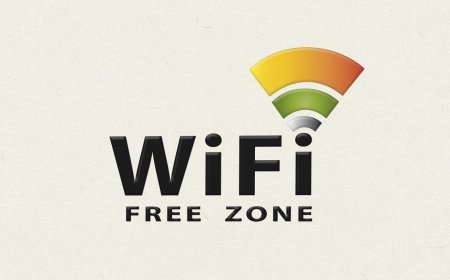बिहार के वैशाली में पुलिस कस्टडी में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस हिरासत में कथित मौत की यह घटना सुप्रीम कोर्ट के करीब एक सप्ताह पहले राजस्थान में ऐसी मौतों पर राज्य सरकार से जवाब तलब के बाद हुई है। यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौतों को लेकर जवाब तलब किया है। इससे पहले भी ऐसी मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट गाइड लाइन जारी कर चुका है। इसके बावजूद देश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पुलिस हिरासत में मौतों को लेकर स्वत: संज्ञान लिया। देशभर के थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने हिरासत में मौत को लेकर रिपोर्ट पर कहा कि 2025 में पिछले 7-8 महीनों में अकेले राजस्थान में ही पुलिस हिरासत में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि, 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुना चुका है। इसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जाने के निर्देश दिए गए थे। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस सीसीटीवी फुटेज देने से बचती है। इसके पीछे पुलिस की तरफ से कई तरह के कारण बताए जाते हैं, जैसे कि तकनीकी खराबी, फुटेज स्टोरेज की कमी, जांच जारी है या कानूनी प्रतिबंध।
कई मामलों में तो पुलिस ने फुटेज देने से सीधे इनकार कर दिया या जानबूझकर देरी की। अदालत ने साफ कहा था कि थाने का कोई भी हिस्सा निगरानी से बाहर नहीं होना चाहिए। लॉकअप से लेकर मेन गेट, कॉरिडोर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कमरे, ड्यूटी रूम और थाने का पूरा कैंपस सीसीटीवी कवरेज में होना चाहिए। साथ ही, सीबीआई, ईडी, एनआईए, एनसीबी और डीआरआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के दफ्तरों में भी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए थे। इनका डेटा कम से कम एक साल तक सुरक्षित रहे। इन मामलों से यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का पालन पूरी तरह से नहीं किया गया है। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की समीक्षा के लिए बनाई गई केंद्रीय और राज्य स्तरीय कमेटियां भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं।
राजस्थान में लगातार हो रही हिरासत में मौतों ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन मामलों में पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न कराना संदेह पैदा करता है। अदालत ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि राजस्थान में बीते दो साल में पुलिस हिरासत में 20 लोगों की मौतें हुई। लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी को मौत का दोषी नहीं माना गया। इनमें पांच व्यक्तियों की मौत हार्ट अटैक से होना बताया गया जबकि एक व्यक्ति ने कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया था। दो मामलों में संतरियों को 17 सीसी के नोटिस थमाए गए हैं। शेष 14 मामलों में अभी तक मौत का कोई कारण सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि इन मामलों की जांच करवाई जा रही है। पुलिस हिरासत में मौतों की खबर भारत में जैसे बहुत आम है। लगभग रोज़ अख़बारों में जेल में या पुलिस की हिरासत में मारे जाने वालों की ख़बर छपती है। 26 जुलाई 2022 को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि 2020 से 2022 के बीच 4484 लोगों की मौत हिरासत में हुई थी। मानवाधिकार आयोग ने माना कि 2021-22 में जेलों में 2152 लोग मारे गए। इनमें 155 मौतें पुलिस हिरासत में हुई थीं। लेकिन सवाल है, देश में हिरासत में इतनी मौतें क्यों होती हैं? क्या पुलिस व्यवस्था हिरासत में या जेल काट रहे क़ैदियों के साथ अमानवीय बरताव करती है? क्या वह क़ानूनों का खय़ाल नहीं रखती? कॉमन कॉज के एक सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर पुलिसवाले टॉर्चर और हिंसा को अपने काम के लिए ज़रूरी मानते हैं। 30 फ़ीसदी पुलिसवाले गंभीर मामलों में थर्ड डिग्री टॉर्चर को सही मानते हैं। जबकि 9 फीसदी यहां तक मानते हैं कि छोटे-मोटे अपराधों में भी ये सही है।
प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी मुठभेड़ों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। न्यायालय ने कहा कि जिन मामलों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ साबित होती है, उन्हें दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम मानते हुए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी गई कि उन्हें मुठभेड़ के नाम पर हत्या करने के लिए इस बहाने से माफ नहीं किया जाएगा कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों या राजनेताओं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों के आदेशों का पालन कर रहे हों। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यातना को संविधान या अन्य दंडात्मक कानूनों में परिभाषित नहीं किया गया है। किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को दी जाने वाली यातना, मूलत: कमज़ोर पर शक्तिशाली की इच्छा को पीड़ा देकर थोपने का एक साधन है। आज यातना शब्द मानव सभ्यता के अंधकारमय पक्ष का पर्याय बन गया है। यातना और अन्य क्रूर अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले 170 देशों में से, भारत उन आठ देशों में से एक है जिन्होंने अभी तक इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन नहीं किया है। अपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, विधेयक में कहा गया है कि इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन भारत सरकार की बुनियादी सार्वभौमिक मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। विधि आयोग की 273वीं रिपोर्र्ट में कहा गया कि हिरासत में मौतें सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं हैं, बल्कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में गहरी अस्वस्थता का लक्षण हैं। संवैधानिक गारंटी, कानूनी सुरक्षा उपायों और न्यायिक घोषणाओं के बावजूद, हिरासत में यातना और दुव्र्यवहार का प्रयोग व्यापक रूप से जारी है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जहाँ किसी लोक सेवक को हिरासत में यातना देना साबित हो जाता है, वहाँ यह साबित करने का भार कि यातना जानबूझकर नहीं दी गई थी, या लोक सेवक की सहमति या सहमति से नहीं दी गई थी, लोक सेवक पर आ जाएगा। आयोग के मसौदे में हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा का भी प्रावधान था। मसौदे में पीडि़त को मुआवज़ा देने का भी प्रावधान था। यह रिपोर्ट धूल चाट रही है। राजनीतिक दलों को ऐसे मामलों में तभी चिंता होती है, जब वे विपक्ष में होते हैं। सत्ता मे आते ही नेता गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस कानूनों में सुधार किया है, किन्तु हिरासत में मौतें और प्रताडऩा जैसे मामलों में जिम्मेदारी तय नहीं की गई और न ही किसी तरह के मुआवजे का ्रप्रावधान किया गया। पुलिस के खिलाफ ऐसे मामलों में जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक हिरासत में मौतों से देश शर्मसार होता रहेगा।
- योगेन्द्र योगी