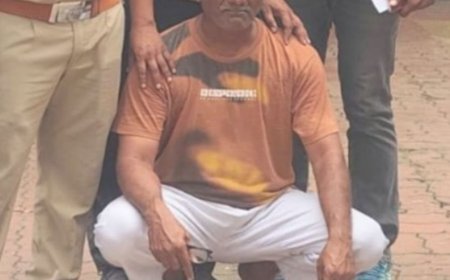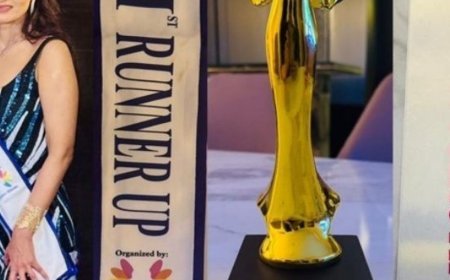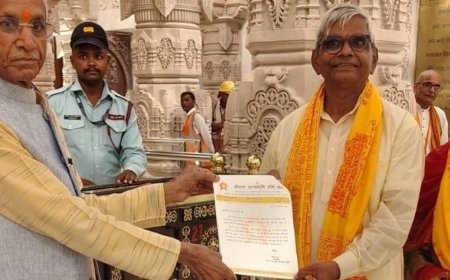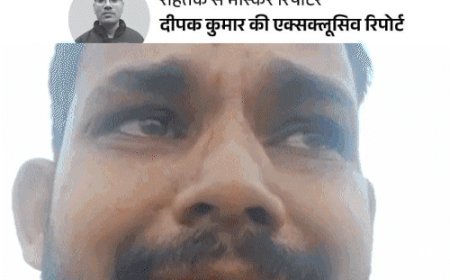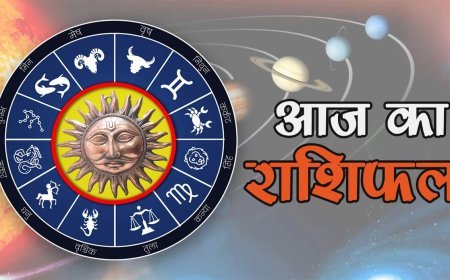सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर दिए गए अपने अंतरिम आदेश में एक बार फिर भारतीय न्यायपालिका की उस परंपरा को दोहराया है, जिसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून को संवैधानिक रूप से वैध मानने की धारणा सर्वोपरि होती है। न्यायालय ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इंकार किया, लेकिन कुछ प्रमुख प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाकर यह संदेश दिया कि कानून बनाने की प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वक़्फ़ परिषदों और बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित रहनी चाहिए। केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य न हों और राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार की सीमा लागू हो। देखा जाये तो यह निर्णय एक संवेदनशील धार्मिक संस्था के चरित्र को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि प्रशासनिक दृष्टि से गैर-मुस्लिम को सीईओ बनाना पूरी तरह असंवैधानिक नहीं है, लेकिन “जहाँ तक संभव हो” मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति ही की जानी चाहिए।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाई, जिसके तहत सरकार किसी भूमि विवाद के दौरान वक़्फ़ संपत्ति को डिरेकोग्नाइज़ कर सकती थी। यह प्रावधान ‘separation of powers’ (शक्तियों का पृथक्करण) के सिद्धांत के विरुद्ध माना गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संपत्ति का अधिकार और स्वामित्व तय करने का अधिकार केवल न्यायाधिकरणों और अदालतों का है, न कि कार्यपालिका का। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जब तक विवाद का अंतिम निपटारा नहीं होता, तब तक वक़्फ़ भूमि पर कोई तृतीय पक्ष अधिकार न बनाया जाए।
हम आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने इस आदेश में एक बुनियादी सिद्धांत रेखांकित किया— संसद के कानूनों को ‘prima facie’ वैध मानना चाहिए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उन पर रोक लगनी चाहिए। यह विचार लोकतंत्र में संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की निगरानी—दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है।
देखा जाये तो यह आदेश केवल वक़्फ़ कानून तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक विमर्श का हिस्सा है, जिसमें धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन, अल्पसंख्यक अधिकारों और संविधानिक संतुलन के प्रश्न जुड़े हैं। भारत जैसे बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक समाज में कानून बनाना मात्र एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द का संवेदनशील प्रयास भी है।
फैसले को देखें तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न तो वक़्फ़ बोर्डों की स्वायत्तता को पूरी तरह नकारता है और न ही सरकार को असीमित अधिकार देता है। यह एक संवैधानिक सेफगार्ड है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून न्याय की कसौटी पर खरे उतरें। अंतिम सुनवाई में जो भी फैसला आएगा, वह न केवल वक़्फ़ संस्थानों के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि भारत में धार्मिक संपत्तियों और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए।
- नीरज कुमार दुबे