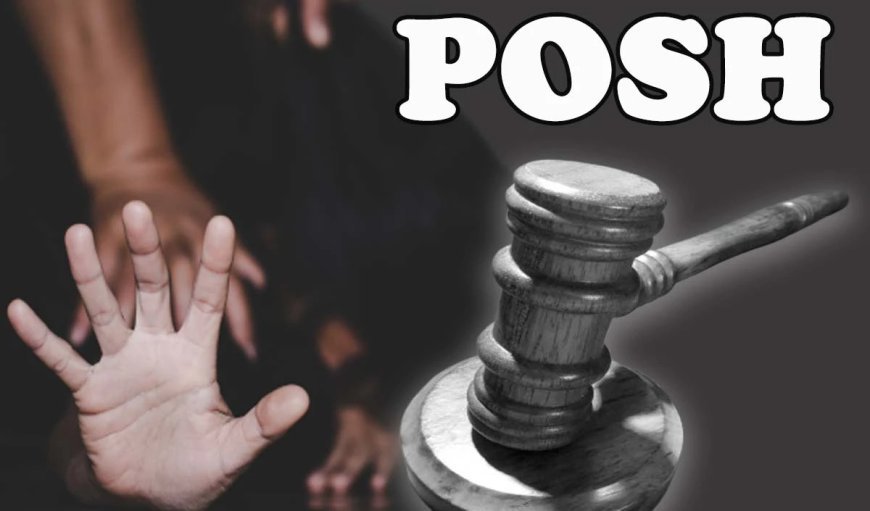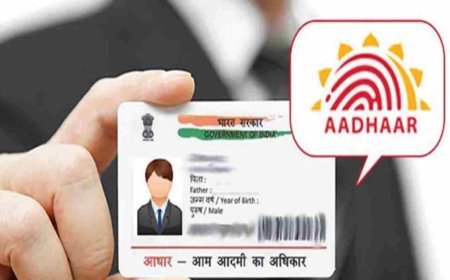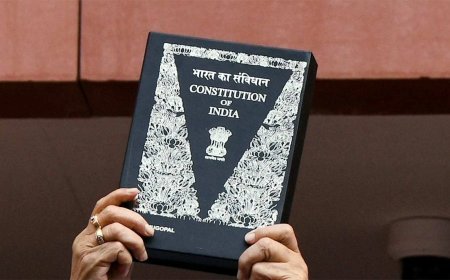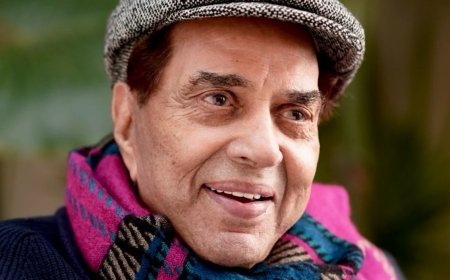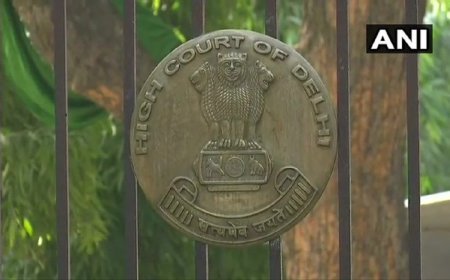राजनीतिक दलों को महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा संबंधी कानून प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट (पॉश एक्ट), 2013 से प्राप्त वैधानिक छूट किसी नैतिक विडंबना से कम नहीं है, चाहे इसका विधिक कारण कुछ भी हो! यह हमारी संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की नैतिक लापरवाही या खामोशी दोनों का नतीजा है? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह तर्क कि राजनीतिक दल और उनके सदस्यों के बीच पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध नहीं होता है, किसी के गले नहीं उतरता है। यह अनुभव की व्यवहारिक कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता है।
यह ठीक है कि उनके बीच पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं होता, लेकिन दफ्तर और कार्यसंस्कृति दोनों होती है। यहां तक कि टूर के दौरान ठहरने वक्त नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं का कमरा आसपास ही रखा जाता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इससे राजनीतिक दलों व उनके नेताओं को कार्यकर्ताओं के शोषण का अंतहीन अधिकार मिल जाता है! खासकर, जब केंद्र और विभिन्न राज्यों की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आदि दल किसी कॉरपोरेट शैली से संचालित होती हों, उनके जनसंपर्क यानी प्रचार-प्रसार व कार्यसंचालन का तरीका लगभग वही हो, जब निर्वाचित राजनेताओं के धन भी पांच वर्ष में ही दुगुने-तिगुने से ज्यादा बढ़ जाते हों, जब राजनेताओं व उनके करीबी संगठन के नेताओं पर महिलाओं के शारीरिक शोषण के अनेक आरोप लगते आए हों, वैसे परिदृश्य में सियासी दलों और सियासतदानों को प्राप्त विधिक छूट उनके गलत इरादों को लीगल प्रश्रय नहीं देना है तो क्या है, यक्ष प्रश्न है?
भारत के अधिकांश लोगों को पता है कि देश की कानून निर्मात्री संस्था 'संसद', विधानसभा मंडलों में बैठे राजनेतागण खुद को 'अभिजात्य प्राणी' समझते हैं और खुद के फंसने वाला कानून कभी नहीं बनाते। वहीं, अपना सियासी हित साधने के लिए प्रायः द्विअर्थी कानून बनाते हैं। वाकई एक ही प्रवृति के विषयों में अस्पष्ट कानूनों की वजह से ही देश अमेरिका की भांति वकीलों का स्वर्ग बन चुका है। कोई भी नेता दो जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दो जगहों की मतदाता सूची में नाम निकल जाने पर जानबूझकर बखेड़ा खड़ा किया जाता है। भूमि-भवन-स्वर्ण निवेश सम्बन्धी चीजों, शिक्षा-स्वास्थ्य-कारोबार आदि में अस्पष्ट कानूनों की वजह से निवेशक मालामाल और उपभोक्ता फटेहाल रहते हैं, आदि।
सबसे बड़ी विडंबना तो यह कि निर्वाचित होते ही, अपराधी/दुष्कर्मी भी 'माननीय' करार दिए जाते हैं। यह स्थिति प्रशासनिक अधिकारियों व न्यायपालिका के लिए भी शर्मनाक है। साथ ही भारतीय बुद्धिजीवियों, सफल पेशेवर समूहों, विश्वविद्यालयों की पवित्र सोच पर करारा तमाचा है। ऐसे में सुलगता हुआ सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट आरक्षण सम्बन्धी कानून और वक्फ बोर्ड कानून आदि में तो संशोधन करने का अधिकार रखता है, लेकिन नेताओं से जुड़े मामलों में उसकी बुद्धिमत्ता/प्रबुद्ध सोच को 'जंग' लग जाती है, सांप सूंघ जाता है जो वैधानिक 'सामाजिक टेटनस/मानसिक विष' जैसे 'जानलेवा रोगों' की वजह बन जाते हैं।
स्वाभाविक सवाल है कि हमारे राजनेता जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, अपनी सैलरी व भत्ता खुद ही बेहिसाब बढ़ा सकते हैं, राजनीतिक चंदा के लिए 'चोर दरवाजे' छोड़ सकते हैं, संसद के भीतर-बाहर कुछ भी अनाप-शनाप बोल सकते हैं, जिससे सामाजिक-राष्ट्रीय हितों पर चोट पहुंचती है, आदि। इनके कार्यकर्ता पाकिस्तान-बंगलादेश का झंडा लहरा सकते हैं, लेकिन इस पर कभी तर्कसंगत बहस नहीं होती! बेलगाम सोशल मीडिया इनका आधुनिक प्रचार हथियार बन चुका है। क्रिप्टो करेंसी इनके अवैध लेन-देन का साधन बन चुका है।लेकिन एक समान कानून की याद इन्हें कतई नहीं आती। इससे आम व्यवसायियों के कारोबारी हित भी प्रभावित होते हैं।
कोढ़ में खाज यह कि अब सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि "राजनीतिक दलों में सदस्यता रोजगार जैसी नहीं है- इसमें न तो नियमित वेतन है और न ही संविदात्मक/नौकरी संबंधी अनुबंध।" सवाल है कि कार्यकर्ता दिन-रात पार्टी की सेवा में लगे रहते हैं या नहीं? इनको मानदेय क्यों नहीं दिया जाता? क्या इसी वजह से ये प्रशासनिक या सामाजिक 'दलाली' करते हैं और किसी तरह निर्वाचित नेताओं के लोकल एजेंट बनकर अपना गुजारा करते हैं। क्या इसी वजह से भ्रष्टाचार, शिष्टाचार नहीं बन गया है? यह कौन नहीं जानता कि अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों/मंत्रियों के बीच दलाली करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ही नेटवर्क 'गर्म गोश्त' की भी दलाली करता है, इसलिए इन्हें भी पॉश एक्ट 2013 के दायरे में लाए जाने की जरूरत है। रहस्य न खुले, इसलिए इस धंधे में एक-दूसरे की जान लेना स्वाभाविक बात है! जिसे प्रशासनिक पहुंच के बल पर दबा दिया जाता है। बावजूद इसके कुछ मामले सुर्खियां बन जाते देखे-सुने जाते हैं।
बताया जाता है कि पॉश (POSH) एक्ट की परिभाषा में वही संगठन आते हैं जहाँ "रोजगार और भुगतान" के आधार पर कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध मौजूद हैं। चूंकि राजनीतिक पार्टी में कोई महिला कार्यकर्ता बनने का अर्थ 'नौकरी' पाना नहीं है, बल्कि यह केवल "मेम्बरशिप" का मामला है, जिसमें औपचारिक रोजगार संबंध स्पष्ट नहीं होता। ऐसे में राजनीतिक दलों के कार्य के दायरे (जैसे रैलियां, जनसंपर्क, अभियान आदि) को कानूनी तौर पर "स्थायी कार्यालय या कार्यस्थल" की तरह चिन्हित नहीं किया जा सकता- यह अत्यंत गतिशील और अस्थिर होते हैं।
वहीं, चूंकि इस क़ानून के प्रभाव और विकल्प असरकारक हैं, इसलिए राजनीतिक दलों को मिला छूट इस कानून की सफलता पर संशय पैदा करता है। इस छूट के कारण यदि किसी महिला राजनीतिक कार्यकर्ता को उत्पीड़न का सामना करना पड़े तो वह पॉश एक्ट 2013 के तहत शिकायत नहीं कर सकती है। हालांकि वह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी/IPC) या किसी अन्य आपराधिक कानून का उपयोग कर सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत किया है कि राजनीतिक दलों को पॉश एक्ट, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने की बाध्यता भी नहीं है। इसलिए स्वाभाविक सवाल है कि राजनीतिक दलों को यह छूट क्यों? क्या वही कानून बनाते-बनवाते हैं, सिर्फ इसलिए!
हालांकि, अन्य देशों में कुछ वैकल्पिक उपाय भी उपलब्ध हैं, जिसका भारत में अनुशरण किया जाना चाहिए। जैसे-कुछ देशों में राजनीतिक दल स्वेच्छा से महिलाओं के लिए आंतरिक आरक्षण या शिकायत व्यवस्था अपनाते हैं, किंतु भारत में कानूनी तौर पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वहीं, राजनीतिक दलों को कार्यस्थल महिला सुरक्षा कानूनों से छूट कोर्ट द्वारा इसलिए दी गई है क्योंकि वहां पारंपरिक वेतनभोगी रोजगार संबंध नहीं पाया जाता और उनकी कार्यप्रणाली "स्थायी दफ्तर" जैसी नहीं होती। इसलिए स्वाभाविक सवाल यह है कि क्या यह एक बिडम्बनात्मक सोच व छूट नहीं है? इस पर देशव्यापी बहस खुद राजनीतिक महिला कार्यकर्ताओं के बीच ही करवायी जानी चाहिए।
बताते चलें कि पॉश एक्ट, 2013 ('कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और प्रतितोष अधिनियम') में 'नियोक्ता' और 'कर्मचारी' की परिभाषा स्पष्ट की गई है, जिसके तहत नियोक्ता की परिभाषा तय है। जैसा कि पॉश एक्ट की धारा 2(जी) में स्पष्ट किया हुआ है, 'नियोक्ता' वह व्यक्ति है जो किसी विभाग, संगठन, प्रतिष्ठान या कंपनी का प्रमुख हो या उसका प्रबंधन, पर्यवेक्षण या नियंत्रण करता हो। यानी संगठन का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति 'नियोक्ता' माना जाता है। जबकि 'कर्मचारी' की परिभाषा भी व्यापक है- इसमें नियमित, अस्थायी, संविदा, प्रशिक्षु, स्वैच्छिक या एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले सभी व्यक्ति आते हैं। वेतन, भत्ते या किसी अन्य प्रकार की पारिश्रमिक या बिना पारिश्रमिक के कार्यरत व्यक्ति भी 'कर्मचारी' की श्रेणी में आते हैं।
इस कानून की मुख्य बातें ये हैं कि 'नियोक्ता' और 'कर्मचारी' की परिभाषा संगठनात्मक संबंध और प्रबंधन के अधिकार से निर्धारित होती है न कि केवल वेतन या रोजगार अनुबंध से। वहीं, पॉश एक्ट, 2013 केवल उन्हीं संस्थाओं पर सीधे लागू होता है, जहाँ यह संबंध स्पष्ट रूप से मौजूद हो। इसप्रकार से पॉश एक्ट में 'नियोक्ता' संगठन के प्रमुख/प्रबंधक और 'कर्मचारी' उस संगठन में किसी भी रूप में (अस्थायी, स्थायी, संविदा आदि) कार्यरत व्यक्ति को कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के हित संरक्षण से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून पर भी राजनीतिक असर पड़ा है, जिसके दुरुपयोग के बावजूद भारतीय संविधान एक मजबूत, जीवंत और अनुकूल दस्तावेज़ है, जो आज भी देश की लोकतांत्रिक, न्यायिक और नैतिक नींव का मुख्य आधार बना हुआ है। इसलिए उम्मीद है कि यहां व्याख्या की जा रही नजरिए से भी अविलंब कानूनी संशोधन किए, करवाये जाएंगे।
कहना न होगा कि संविधान सर्वोच्च कानून है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण करता है और चेक-बैलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। इससे कोई भी व्यक्ति या संस्था विधि से ऊपर नहीं हो सकती, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप के समय भी नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा होती है। जहां तक राजनीतिक दुरुपयोग और संस्थागत सुरक्षा का सवाल है तो संविधान की कुछ धाराओं (जैसे- अनुच्छेद 356) का ऐतिहासिक रूप से दुरुपयोग हुआ है; परंतु सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई फैसले जैसे न्यायिक विराम ऐसे दुरुपयोग पर अंकुश लगाने में सफल रहे हैं, जिससे संविधान की संघीय संरचना सुरक्षित बनी रही है।
हाल के वर्षों में भी देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य संस्थाएं समय-समय पर संविधान के मूल उद्देश्यों की रक्षा के लिए सक्रिय रही हैं, भले ही राजनीतिक दल संविधान को अपने हित के हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यह हमारे संविधान की अनुकूलनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो सराहनीय है। संविधान में लचीलापन है, जिससे समयानुसार जनता की आवश्यकताओं, सामाजिक संतुलन और नये अधिकारों को संशिधनों के द्वारा सम्मिलित किया जा सकता है। वहीं, संविधान राष्ट्रीय एकता, अल्पसंख्यक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन की नींव तैयार करता है, जिससे राजनीतिक उठापटक के बावजूद देश की बुनियादी संरचना अखंड रहती है। इसलिए पॉश एक्ट 2013 के दायरे में राजनीतिक दलों और इस जैसे संगठनों को भी लाये जाने की माकूल कानूनी पहल की जानी चाहिए। इससे महिलाओं के प्रति सुनियोजित आपराधिक सोच में कमी आएगी।
जहां तक संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में तर्क का सवाल है तो संविधान व इसके संरक्षक विधि के शासन, अधिकारों की सुरक्षा, तंत्र की पारदर्शिता और कार्यकारी संरचना को संतुलन देते हैं। न्यायपालिकाएँ और संस्थाएं संवैधानिक व्याख्या कर राजनीतिक हस्तक्षेप पर नियंत्रण रखती हैं। इसके लचीलेपन के चलते समय के साथ संविधान अपनी प्रयोजनशीलता व प्रासंगिकता बनाए रखने में सफल है। अतः, राजनीतिक दवाबों और अस्थाई तौर पर गलत इस्तेमाल के बावजूद, भारतीय संविधान अपनी मूल भावना, संतुलन और स्थायित्व बनाए रखने में सक्षम है- यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति और भारतीय लोकतंत्र का संरक्षण है।
इसलिए महिलाओं के शारीरिक शोषण के मामलों में भी राजनीतिक दलों को पॉश एक्ट 2013 जैसे महत्वपूर्ण कानून के दायरे में लाना बदलते हाई टेक वक्त की मांग है और इससे उन्हें छूट देने से समाज की मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मामलों में नेताओं के बचने की पूरी संभावना मौजूदा कानून में उपलब्ध है, जो सवालों के घेरे में है। इसलिए इसे और अधिक व्यापक व प्रभावशाली बनाने की जरूरत है। यही महिलाओं की मांग भी है।
- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक