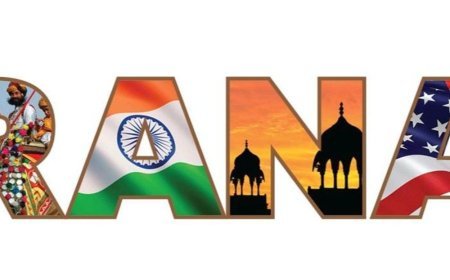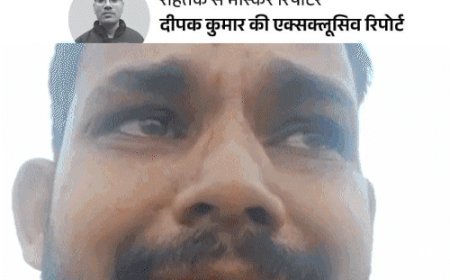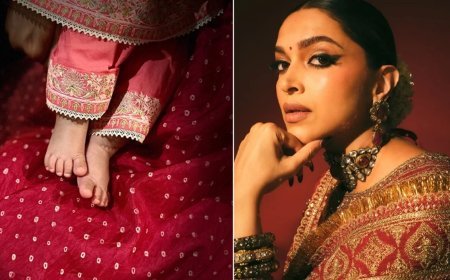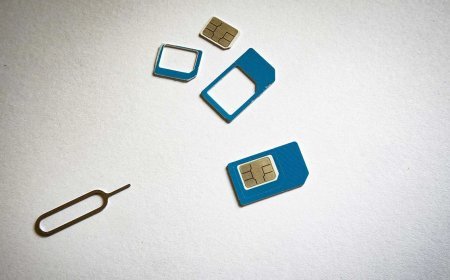लोकतंत्र में किसी भी समाज को अपनी मांगों को सामने रखने और आवाज़ उठाने का पूरा हक है। इसीलिए आरक्षण के सवाल पर मराठा समुदाय की पीड़ा और आकांक्षाओं को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस हक के नाम पर पूरे शहर को बंधक बनाया जा सकता है? मनोज जरांगे का आंदोलन इसी बुनियादी दुविधा को उजागर करता है। हम आपको बता दें कि मनोज जरांगे कई बार अनशन कर चुके हैं और उन पर आरोप है कि उनका आंदोलन कहीं न कहीं राजनीतिक समीकरणों से संचालित है। विपक्ष से नज़दीकी के आरोप और भीड़ जुटाने की रणनीति इस आंदोलन की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।
मगर, इस बार बंबई उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप निर्णायक रहा। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि जरांगे और उनके समर्थक “उल्लंघनकर्ता” हैं और बिना अनुमति के आज़ाद मैदान पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। यह रुख केवल जरांगे के आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र रूप से यह संदेश है कि लोकतंत्र में आंदोलन की स्वतंत्रता और आम नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन अनिवार्य है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर होगी तो न्यायपालिका स्वयं कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।
इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार की कमियां भी उजागर हुईं। 5,000 लोगों की अनुमति के बावजूद 50,000 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा प्रशासनिक विफलता का उदाहरण है। अदालत ने इस पर भी अपनी नाराज़गी जताई। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आंदोलन का अधिकार तभी तक पवित्र है जब तक वह जनजीवन को ठप न करे। न्यायपालिका की सख़्ती ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं की पुनः पुष्टि की है। सामाजिक आंदोलन का रास्ता संवैधानिक होना चाहिए, न कि भीड़तंत्र और दबाव की राजनीति से होकर गुजरना चाहिए। यही संदेश आगे की राजनीति और समाज दोनों के लिए सबसे ज़रूरी है।
सामाजिक टकराव बढ़ सकता है!
देखा जाये तो मुंबई जैसा महानगर, जो देश की आर्थिक धड़कन माना जाता है, वहां जीवन की रफ्तार रुकना केवल स्थानीय समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय भी है। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान सामने आई तोड़फोड़, सड़कों पर जाम और लोगों के साथ अभद्रता की खबरें यह सवाल उठाती हैं कि आखिर सामाजिक आंदोलन और अराजकता की सीमा कहाँ तय होगी। लोकतंत्र में अपनी मांग रखना अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल दूसरों की आज़ादी छीनकर नहीं किया जा सकता।
मनोज जरांगे और उनके समर्थकों का तरीका न केवल आम जनता को असुविधा पहुँचाता है बल्कि आरक्षण जैसे गंभीर प्रश्न को भी भावनात्मक उग्रता की भेंट चढ़ा देता है। समाज को आरक्षण के नाम पर भटकाना और इसे राजनीतिक सौदेबाज़ी का औज़ार बना देना, वास्तविक सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करता है। इस तरह की रणनीति का असर यह होता है कि जो सवाल शांति और तर्क से सुलझाए जाने चाहिए, वह टकराव और तनाव में बदल जाते हैं।
सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऐसे आंदोलन समाज के भीतर विभाजन की दीवार खड़ी करते हैं। आरक्षण की मांग को लेकर जब एक समुदाय दूसरे के खिलाफ खड़ा होता है तो राष्ट्रीय एकता की भावना आहत होती है। भारत की ताक़त विविधता में एकता है, लेकिन जब राजनीतिक या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए समाज को बांटने का प्रयास होता है, तो यह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि सामाजिक सौहार्द पर भी चोट करता है।
इसलिए यह आवश्यक है कि आरक्षण जैसी संवेदनशील नीतियों पर बहस और निर्णय संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हों। आंदोलन का रास्ता संवैधानिक होना चाहिए, न कि तोड़फोड़, हिंसा या दबाव की राजनीति से होकर गुजरना चाहिए। मुंबई की घटनाओं ने एक बार फिर हमें सचेत किया है कि यदि समय रहते ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो सामाजिक न्याय के नाम पर अराजकता और विभाजन की राजनीति ही हावी होगी, जो राष्ट्रहित के विपरीत है।
इसके अलावा, अब यह भी दिख रहा है कि मराठा आरक्षण का सवाल केवल एक समुदाय की मांग भर नहीं रह गया है, बल्कि यह महाराष्ट्र की राजनीति और समाज दोनों के लिए गहरी जटिलताओं का स्रोत बन चुका है। मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा समाज लगातार दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी ओर ओबीसी समुदाय और उसके नेता छगन भुजबल खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। यही विरोध अब महाराष्ट्र सरकार के लिए नए सिरदर्द का कारण बनता दिखाई दे रहा है।

भुजबल का तर्क साफ़ है कि यदि मराठा समाज को ओबीसी के हिस्से में आरक्षण दिया गया तो यह अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर सीधा अतिक्रमण होगा। ओबीसी समुदाय पहले से ही शिक्षा और नौकरियों में अपने हिस्से को लेकर सजग और संवेदनशील है। ऐसे में यदि उन्हें लगे कि उनका कोटा घटाया जा रहा है, तो उनके भीतर असंतोष और आक्रोश तेजी से भड़क सकता है। यह स्थिति न केवल सामाजिक टकराव को जन्म देगी बल्कि राजनीतिक समीकरणों को भी अस्थिर कर देगी।
महाराष्ट्र सरकार पहले से ही दोहरी दबाव की स्थिति में है। एक ओर मराठा समुदाय, जो राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है, उसकी मांगों को अनदेखा करना आसान नहीं है। दूसरी ओर, ओबीसी समुदाय का विरोध भी नज़रअंदाज़ करना सरकार के लिए जोखिम भरा है क्योंकि यह समुदाय संख्या और प्रभाव दोनों के लिहाज़ से मजबूत है।
वहीं छगन भुजबल का रुख यह संकेत देता है कि आने वाले समय में यह मुद्दा केवल आरक्षण की कानूनी बहस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक ध्रुवीकरण और जातीय टकराव को भी हवा देगा। सरकार यदि किसी एक पक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश करेगी तो दूसरा पक्ष नाराज़ होकर सड़कों पर उतर सकता है। यह स्थिति राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव, दोनों को जन्म दे सकती है।

देखा जाये तो छगन भुजबल और ओबीसी समुदाय का विरोध महाराष्ट्र सरकार के लिए दो धार वाली तलवार है— मराठा समुदाय को पूरी तरह संतुष्ट करना मुश्किल है और ओबीसी को नाराज़ करना खतरनाक। यही दुविधा इस आरक्षण विवाद को और पेचीदा बनाती है।
महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की साजिश तो नहीं?
देखा जाये तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का सवाल लंबे समय से सामाजिक-राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। परंतु हाल के वर्षों में यह मुद्दा केवल सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य की सत्ता-समीकरणों को हिलाने वाले राजनीतिक औज़ार के रूप में भी बार-बार उभरा है।
भाजपा–शिवसेना (शिंदे गुट) और अजित पवार की एनसीपी वाली गठबंधन सरकार पहले ही आपसी तालमेल और राजनीतिक संतुलन साधने की चुनौती से जूझ रही है। ऐसे में मराठा आरक्षण का आंदोलन विपक्ष के लिए एक ऐसा हथियार बन सकता है, जिससे न केवल सरकार पर दबाव बढ़े बल्कि उसके भीतर अविश्वास और मतभेद भी गहराए। जब भी आंदोलन तेज होता है, तब सरकार को प्रशासनिक मजबूती की बजाय समझौते और बचाव की मुद्रा में खड़ा होना पड़ता है। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से शासन-प्रशासन को पंगु बनाती है।
इसके अलावा, बार-बार आंदोलन के कारण राज्य का विकास भी प्रभावित होता है। उद्योग और निवेश का माहौल अनिश्चित हो जाता है, कानून-व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और आम नागरिक का जीवन अस्त-व्यस्त होता है। जिस मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां जब सड़कों पर तोड़फोड़ और जाम की स्थिति पैदा होती है तो यह सीधा संदेश जाता है कि महाराष्ट्र राजनीतिक अस्थिरता और जातीय खींचतान का शिकार है। यह छवि राज्य के दीर्घकालिक विकास को बाधित करती है।
इसके अलावा, राजनीतिक साजिश की आशंका इसलिए भी मजबूत होती है क्योंकि आंदोलन बार-बार तब तेज होते हैं जब सरकार के सामने कोई बड़ा राजनीतिक या प्रशासनिक एजेंडा होता है। यह संयोग मात्र नहीं हो सकता कि आंदोलन हर बार उस वक्त उग्र हो जब सत्ता पक्ष अपनी स्थिति मजबूत करने या विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करता है।
देखा जाये तो मराठा आरक्षण की वास्तविक मांग चाहे कितनी भी जायज़ क्यों न हो, इसके इर्द-गिर्द खड़ी होने वाली बार-बार की उग्रता और राजनीति यह संकेत देती है कि इसे केवल सामाजिक आंदोलन नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे सत्ता को अस्थिर करने और विकास की गति को रोकने की राजनीतिक साज़िश की परछाईं साफ़ दिखाई देती है।
अदालत चुस्त, सरकार सुस्त!
इसके अलावा, मराठा आरक्षण आंदोलन ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब सरकार निर्णय लेने में ढुलमुल रवैया अपनाती है तो क्या अदालतों को प्रशासनिक भूमिका निभानी पड़ती है? हालिया घटना में बंबई उच्च न्यायालय ने जिस तरह सख्ती दिखाई और जनजीवन बाधित होने पर सीधे हस्तक्षेप किया, उसने आम नागरिकों को राहत तो दी, लेकिन साथ ही एक नई बहस भी शुरू कर दी है।
देखा जाये तो लोकतंत्र में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के हितों की रक्षा करे और प्रशासन को चुस्त रखे। मगर महाराष्ट्र सरकार ने आंदोलनकारियों को न तो समय पर नियंत्रित किया, न ही व्यवस्था बनाने में कोई कठोरता दिखाई। सरकार की यह राजनीति कि “किसी को नाराज़ न किया जाए” आम जनता की कठिनाइयों को बढ़ाती है। नतीजा यह हुआ कि न्यायपालिका को सख्त कदम उठाने पड़े और सड़क से लेकर अदालत तक आंदोलनकारियों पर दबाव डालना पड़ा।

लेकिन क्या यह अदालत का काम है? संविधान ने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग-अलग भूमिकाएँ दी हैं। यदि अदालतों को बार-बार प्रशासनिक आदेश देने पड़ें— जैसे भीड़ हटाना, सड़कों से जाम साफ़ कराना, या आंदोलन नियंत्रित करना तो यह असल में सरकार की विफलता का प्रमाण है। लोगों की अपेक्षा यह है कि अदालत कुछ ठोस दिशानिर्देश बनाए ताकि भविष्य में आंदोलनों के नाम पर शहर बंधक न बनें। मगर दीर्घकालिक समाधान केवल अदालत से नहीं आएगा। समाधान तब निकलेगा जब सरकार राजनीतिक साहस दिखाए, स्पष्ट नीति अपनाए और यह सुनिश्चित करे कि आंदोलन का अधिकार जनता की स्वतंत्रता और शहरी जीवन की सामान्य गति पर भारी न पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं कि अदालत की सख्ती ने जनता को तात्कालिक राहत दी है, लेकिन यह भी याद रखना होगा कि न्यायपालिका “प्रशासनिक विकल्प” नहीं हो सकती। जिम्मेदारी अंततः सरकार की ही है कि वह निर्णय ले, दृढ़ता दिखाए और जनजीवन को बाधित होने से बचाए।
बहरहाल, लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है, लेकिन यह अधिकार कानून और संविधान की सीमाओं के भीतर ही मान्य है। मनोज जरांगे और उनके जैसे आंदोलनकारी जब भीड़ जुटाकर सड़कों पर कब्ज़ा करते हैं, जनजीवन को ठप कर देते हैं और न्यायालय तक की घेराबंदी करने से पीछे नहीं हटते, तो यह लोकतांत्रिक आंदोलन नहीं बल्कि भीड़तंत्र का रूप ले लेता है। ऐसे उदाहरण समाज और शासन दोनों के लिए खतरनाक संकेत हैं। समाज को यह समझना होगा कि आंदोलनकारी तभी ताक़तवर बनते हैं जब भीड़ उनके पीछे खड़ी होती है। यदि आम नागरिक यह ठान ले कि किसी भी आंदोलन को समर्थन तभी देंगे जब वह शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढांचे में हो, तो ऐसे नेताओं की “भीड़ की राजनीति” स्वतः कमजोर हो जाएगी। मीडिया और नागरिक समाज को भी चाहिए कि अराजकता फैलाने वाले आंदोलनों को महिमा मंडित करने की बजाय उनकी असली तस्वीर सामने रखें।
साथ ही, कानून का कठोर और निष्पक्ष उपयोग भी आवश्यक है। यदि आंदोलनकारी नियम तोड़ते हैं, तो उनके खिलाफ आर्थिक दंड, अवमानना की कार्रवाई और गिरफ्तारी जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। जब तक कानून का डर वास्तविक नहीं होगा, तब तक ऐसे लोग बार-बार भीड़ के सहारे सत्ता और प्रशासन को चुनौती देते रहेंगे। सबसे बड़ा सबक समाज तभी सिखा सकता है जब जनता साफ़ संदेश दे कि अधिकार की लड़ाई का रास्ता केवल संविधान और न्यायपालिका से होकर जाता है, न कि भीड़ और दबाव से। लोकतंत्र में भीड़ की ताकत क्षणिक होती है, लेकिन कानून और जनमत की ताकत स्थायी होती है। मनोज जरांगे जैसे आंदोलनकारियों को यही एहसास कराना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।
-नीरज कुमार दुबे