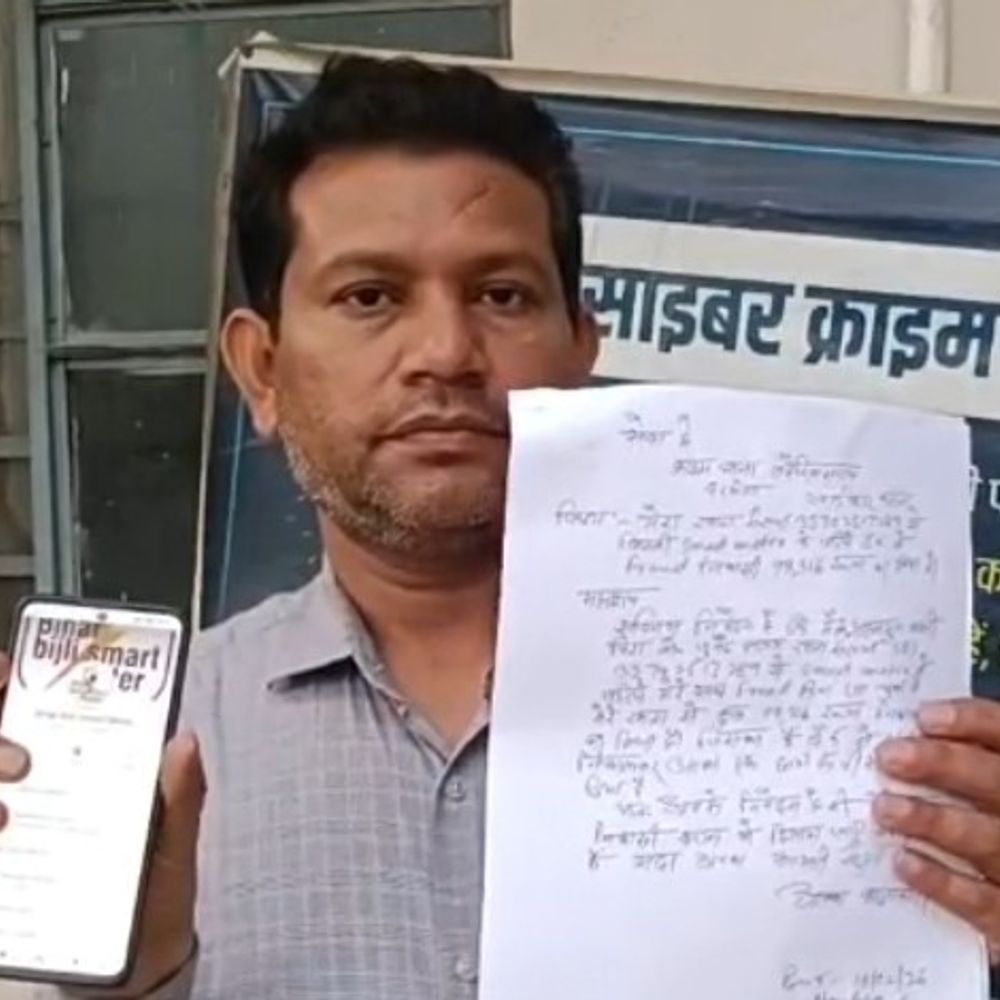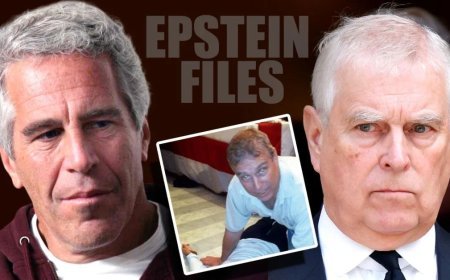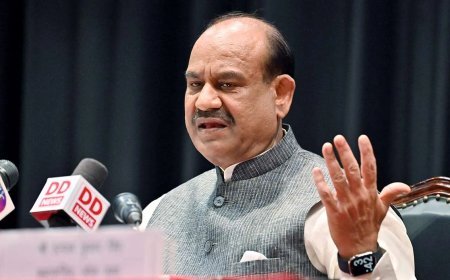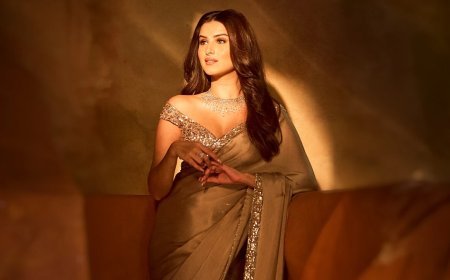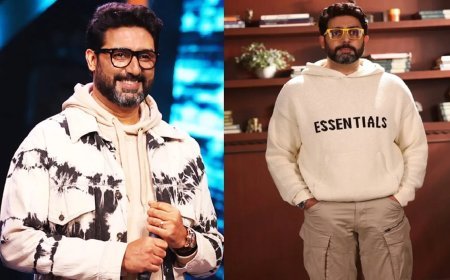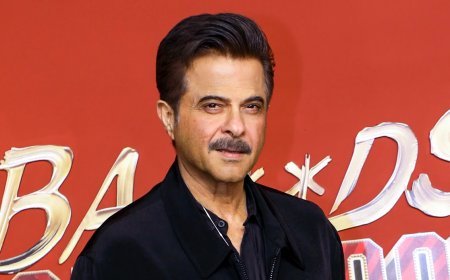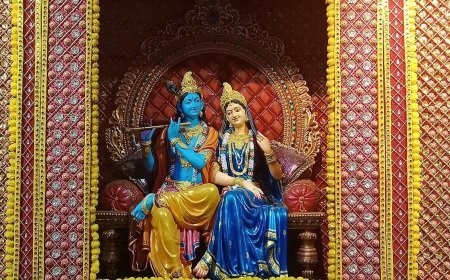भले ही भारतीय संविधान ने देश-काल-पात्र के परिप्रेक्ष्य में हम भारतीयों को बहुत कुछ दिया है, फिर भी इससे और अधिक लेने की अपेक्षा रखना लाजिमी है। इस दिशा में सुलगता हुआ सवाल यही है कि आखिर सिस्टम पर विगत लगभग आठ दशकों से कुंडली मार कर बैठने वाले लोगों या उनके उत्तराधिकारियों-परिजनों ने, जिसमें संविधान की आरक्षण व्यवस्था द्वारा पैदा किये हुए राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक और मीडियागत के 'अभिजात्य वर्गों' के विधिक शोषण से उनके ही वर्ग या समाज के संघर्षरत अन्य लोगों को आखिर मुक्ति कब तक मिलेगी!
इतना ही नहीं, नियम कानून द्वारा इस देश में असली समाजवाद, समानतावाद और समरसतावाद कब तक लाया जाएगा? वहीं, पूरी व्यवस्था पर हावी होते परिवारवाद और सम्पर्कवाद को कब और कैसे हतोत्साहित किया जाएगा? चाहे अल्पसंख्यक वाद हो या पंथनिरपेक्षता/धर्मनिरपेक्षता का सवाल, इसे व्यवहारिक अमलीजामा कब तक पहनाया जाएगा? वहीं, पाकिस्तान-बंगलादेश के मुकाबिल इसे तुलनात्मक रूप से कबतक लागू करवाया जाएगा?
खास बात यह कि इस दिशा में सहयोगी साबित हो रहे द्विअर्थी कानूनों को आखिर कैसे और कबतक बदला जाएगा? वहीं, बहुमतधारी राजनेताओं द्वारा अल्पमत का धड़ल्ले से किये जा रहे उत्पीड़न को आखिर कैसे रोका जाएगा? वहीं, योग्यता के ऊपर अयोग्यता को कबतक थोपा जाता रहेगा? क्योंकि किसी भी सभ्य व सुसंस्कृत समाज में ऐसी विधिक विडंबनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा और मेरे जैसे लोगों का स्पष्ट मानना है।
साथ ही, पेशेवर संस्थाओं को भी क्षुद्र सियासत के मकड़जाल से शीघ्र मुक्त करवाना भी बदलते वक्त की मुखर मांग है, ताकि नीतिगत घालमेल को रोका जा सके। यही वजह है कि भारतीय संविधान में व्यापक सुधार के लिए कतिपय प्रमुख संशोधन बहुत जरूरी समझे जा रहे हैं।प्रासंगिक सवाल है कि आखिर भारतीय संविधान से अपेक्षित मौलिक संशोधन कबतक होंगे? यहां पर विस्तार पूर्वक समझिए कि ये अब कितने जरूरी बन चुके हैं? क्योंकि कानूनी स्थितियों के लाभ उठाते हुए कुछ अमीर लोग भी वास्तविक दलितों-पिछड़ों के हक मार रहे हैं। इसलिए कतिपय संवैधानिक सुधार बहुत जरूरी समझे जाते हैं।
दरअसल, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि वर्तमान समय की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के अनुरूप पूछा जा सके। संशोधन प्रक्रिया में लचीलापन बढ़ाकर संविधान को और अधिक सामयिक बनाया जा सकता है। तत्सम्बन्धी बहुमूल्य सुझावों पर गौर किया जाना चाहिए, जिनमें निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं:-
पहला, संविधान में संशोधन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाना चाहिए, ताकि राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जा सके। संवैधानिक संशोधनों में नागरिक समाज और विभिन्न दलों की भागीदारी सुनिश्चित हो। वहीं, नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में और मजबूती देने तथा उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को बेहतर तरीके से संवैधानित किया जा सके।
दूसरा, मौलिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना जरूरी बताया गया है, साथ ही नागरिक स्वतंत्रताओं को मजबूत करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सुधारा जाना चाहिए। संविधान के मूल ढांचे की रक्षा के साथ-साथ वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों में सुधार आवश्यक है, जैसे कि मौलिक अधिकारों का सशक्तीकरण एवं आपातकालीन प्रावधानों की सीमाओं का पुनः मूल्यांकन। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक नैतिकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से संवैधानिक नैतिकता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
तीसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका सुधारों की मांग है, ताकि संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण प्रभावी तरीके से हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों को मजबूत करना, साथ ही न्यायालयों की कार्यप्रणाली को तीव्र और प्रभावी बनाना आवश्यक है।
चतुर्थ, संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, ताकि स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान हो सके और केंद्र के अतिक्रमण को रोका जा सके। संघीयता के संतुलन को सुधारने हेतु केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पुनर्वितरण आवश्यक है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता और निर्णायक शक्तियाँ बढ़ सकें तथा संघीय संकट कम हो।
पंचम, सामाजिक न्याय और समावेशन के लिए विशेष वर्गों के अधिकारों की पुनः समीक्षा, जिससे वे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप रहें और सामाजिक एकता बनी रहे।
छठा, डिजिटल युग में संविधान की प्रासंगिकता बनाए रखने हेतु नई तकनीकों को ध्यान में रखते हुए डेटा सुरक्षा, निजता और सूचना के अधिकार जैसे विषयों पर नए प्रावधान शामिल किए जाएं।
सप्तम, आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संवैधानिक व्यवस्था में स्पष्ट और सीमित प्रावधान रखने की सलाह दी जाती है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा हो सके।
मेरा स्पष्ट मानना है कि ये बहुमूल्य सुझाव भारतीय संविधान को अधिक गतिशील, समावेशी और समय के साथ विकसित होते रहने वाला दस्तावेज़ बनाएंगे, जिससे यह देश के लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए बेहतर कार्य करेगा। ये सुझाव संविधान की गतिशीलता और प्रभावशीलता बढ़ाने के साथ ही लोकतांत्रिक और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक माने जा रहे हैं। संविधान की समय-समय पर समीक्षा एवं आवश्यक संशोधन इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं।
# भारतीय संविधान में प्राथमिकता के साथ अपेक्षित संशोधन निम्नलिखित हो सकते हैं-:-
जहां तक भारतीय संविधान में प्राथमिकता के साथ संशोधन किए जाने वाली संवैधानिक धाराओं का सवाल है तो उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं: पहला, अनुच्छेद 19 (मौलिक अधिकार) की धाराएं, खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी धाराएं, जिन्हें सामाजिक व राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उचित संशोधनों की आवश्यकता है।
दूसरा, अनुच्छेद 368, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ताकि संशोधन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, लचीली और लोकतांत्रिक बने।
तीसरा, अनुच्छेद 15, 16, और 17, जो समानता और सामाजिक न्याय से संबंधित हैं, इनका संशोधन सुनिश्चित करता है कि सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा बनी रहे।
चतुर्थ, अनुच्छेद 85, 87, 174, 176, 341, और 342, जो संसदीय सत्र, राज्यों के पहचान और विशेष दर्जे से संबंधित हैं, जिन्हें संघीय संतुलन के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
पंचम, अनुच्छेद 124A (राजद्रोह) और संबंधित धारा 153A, 295A, 505 दंड संहिता के, जो कानून और व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील प्रावधान हैं, इनमें संशोधन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
मेरा स्पष्ट मानना है कि उपर्युक्त कुछेक धाराएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके संशोधन से मौलिक अधिकारों की रक्षा, संघीयता का सटीक संतुलन, और संवैधानिक प्रक्रिया की मजबूती सुनिश्चित होती है। साथ ही, संविधान की बुनियादी संरचना को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित रहें।
# मौलिक अधिकारों में संशोधन की आवश्यकता
जहां तक मौलिक अधिकारों में संशोधन की आवश्यकता का सवाल है तो यह बताया जाता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन मुख्य रूप से उन धाराओं में होती है जो समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप नहीं रह पातीं या जिनमें स्पष्टता, सुरक्षा, और नागरिकों के अधिकारों की मजबूती की जरूरत होती है। इस दृष्टिकोण से मुख्य संशोधन की ज़रूरत निम्नलिखित धाराओं में महसूस की जाती ती है:
पहला, अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार): इसे समय के बदलते सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य से जुड़े खतरों के मद्देनज़र और अधिक व्यापक और विस्तृत बनाने की जरूरत है।
दूसरा, अनुच्छेद 19 (मुक्ति के अधिकार): विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नए सामाजिक और डिजिटल युग के संदर्भ में सीमाओं और जिम्मेदारियों के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है।
तीसरा, अनुच्छेद 15, 16 और 17 (भेदभाव की निषेध और समानता से संबंधित प्रावधान): सामाजिक न्याय और समावेशन के लिए इन धाराओं को और मजबूत करने और आधुनिक सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए संशोधन आवश्यक हैं।
चतुर्थ, अनुच्छेद 32 (नागरिकों को न्यायालयों के समक्ष मूल अधिकारों का संरक्षण): इसे और अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने की जरूरत है ताकि नागरिकों को समय पर संरक्षण मिल सके।
पंचम, अनुच्छेद 25 से 28 (धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान): धर्मनिरपेक्षता की भूमिका को बचाए रखने के लिए इन धाराओं को संवैधानिक संदर्भ में पुनः स्पष्ट करना जरूरी है। सामाजिक, तकनीकी और वैश्विक चुनौतियों के चलते इन धाराओं के संशोधन से मौलिक अधिकारों को आधुनिक परिस्थिति के अनुरूप सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे संविधान की प्रासंगिकता और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
# भारतीय संविधान संशोधन की वैधानिक प्रक्रिया
बताते चलें कि भारतीय संविधान संशोधन की वैधानिक प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित है। इसमें संशोधन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और उसे दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। वहीं, संघीय ढांचे से संबंधित संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक होती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति की मंजूरी से संशोधन विधि रूप में लागू होता है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति को विधेयक को रोकने या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजने का अधिकार नहीं है।
विधिक बाधाओं में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के "मूल ढांचे" का सिद्धांत स्थापित किया है, जिसके अनुसार कोई भी संशोधन यदि संविधान के मूल स्वरूप को बदल देता है, वह अमान्य माना जाएगा। न्यायपालिका के पास संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जिससे वह यह तय कर सकती है कि संशोधन संविधान के मूल तत्त्वों के अनुकूल है या नहीं। इस न्यायिक समीक्षा ने संसद के संशोधन अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण सीमा लगाई है।
इसके अलावा, संशोधन प्रक्रिया की कठोरता भी एक बाधा है क्योंकि कई आवश्यक सुधारों और संशोधनों को पारित करने में इसे चुनौतीपूर्ण बना देती है। कभी-कभी राजनीतिक मतभेद और राज्यों की असहमति भी प्रक्रिया को धीमा कर देती है। परिणामी रूप से संविधान में आवश्यक बदलाव समय से नहीं हो पाते या विवाद का विषय बन जाते हैं। इस प्रकार, संविधान में संशोधन की वैधानिक प्रक्रिया सुदृढ़ और न्यायिक रूप से नियंत्रित है, जबकि इसके सामने विधिक और राजनीतिक बाधाएं भी मौजूद हैं जिन्हें संतुलित रूप से संभालना अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधांशु कुमार चौधरी बताते हैं कि संशोधन प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का प्रभाव यह होता है कि कोर्ट संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करता है और संशोधनों की न्यायिक समीक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि संसद को संविधान संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है, जिसका विस्तार प्रस्तावना तक है। हालाँकि, यह संशोधन संविधान के "मूल स्वरूप" या "मूल संरचना" को प्रभावित नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर, 42वें संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने की वैधता को कोर्ट ने बरकरार रखा, यह मानते हुए कि ये शब्द संविधान की मूल संरचना को नहीं बदलते।
वहीं, कोर्ट ने संशोधन प्रक्रिया को एक जीवंत दस्तावेज बनाए रखने के दृष्टिकोण से देखा और संसद को इसका अधिकार दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संशोधन प्रस्तावों में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुधार संविधान के मूल सिद्धांतों के उल्लंघन के बिना हों। इससे संविधान की स्थिरता और लोकतांत्रिक असर दोनों का संतुलन बना रहता है। कोर्ट की यह भूमिका संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और संसद के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने में महत्त्वपूर्ण है।
# संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसलों की सूची में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं:
पहला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): सुप्रीम कोर्ट ने "मूल संरचना सिद्धांत" स्थापित किया कि संसद संविधान में ऐसे संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को बदल दें।
दूसरा, गोलकनाथ मामला (1967): इस फैसले में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों को संविधान में संशोधन के माध्यम से कम नहीं कर सकती।
तीसरा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980): कोर्ट ने केशवानंद भारती के मूल संरचना सिद्धांत को पुनः पुष्टि दी और कहा कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।
चतुर्थ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951): संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति दी गई जिसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन शामिल हैं।
पंचम, संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (2024): सुप्रीम कोर्ट ने 97वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया जो राज्यों की सहकारी समितियों की शक्तियों को प्रभावित करता था।
षष्टम, प्रस्तावना में संशोधन (42वां संशोधन): कोर्ट ने 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़े जाने को वैध माना और इसे संविधान की मूल संरचना के साथ संगत बताया।
सप्तम, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975): न्यायालय ने संसद की संशोधन शक्ति पर कुछ सीमाएं लगाईं, खासकर चुनाव संबंधित प्रावधानों में।
अष्टम, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1993): राष्ट्रपति की धारा 356 के प्रयोग को सीमित किया और धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना माना। ये निर्णय भारतीय संविधान की स्थिरता, लोकतांत्रिक संरचना, और नागरिक अधिकारों की रक्षा में आधारशिला साबित हुए हैं।
# विभिन्न संविधान संशोधनों का नागरिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जो उनके अधिकारों, कर्तव्यों और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है।
पहला, विस्तार और संरक्षण: कई संशोधनों ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तार किया और उन्हें और अधिक सुरक्षित बनाया, जैसे कि महिला, दलित, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण बढ़ाना।
दूसरा, सामाजिक न्याय और आरक्षण: संविधान में आरक्षण संबंधी संशोधनों ने समाज के पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी के अवसर दिए, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला।
तीसरा, लोकतांत्रिक भागीदारी: संशोधनों ने चुनावी प्रक्रिया, मताधिकार और प्रतिनिधित्व के क्षेत्रों में सुधार किया, जिससे नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी और सरकार पर जवाबदेही बढ़ी।
चतुर्थ, नीति निर्देशक सिद्धांत: संवैधानिक संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को सशक्त करते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मददगार साबित हुए, जिससे गरीबों और वंचितों के लिए सरकारी नीतियों का विकास हुआ।
पंचम, आपातकालीन प्रावधानों का प्रभाव: कुछ संशोधनों ने आपातकालीन दौरान नागरिकों के अधिकारों को अस्थाई रूप से सीमित किया, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
छठा, न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधार: न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रशासनिक प्रणाली के सुधार से नागरिकों को निष्पक्ष न्याय और बेहतर सरकारी सेवाएं प्राप्त हुईं।
इस प्रकार, संविधान संशोधनों ने नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हुए समावेशी, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में योगदान दिया है।
# संवैधानिक निर्देशक सिद्धांतों का सवाल
जहां तक, संवैधानिक निर्देशक सिद्धांतों का सवाल है तो इसका सामाजिक असर व्यापक और गहरा रहा है। ये सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित हैं और इसका मूल उद्देश्य है एक सामाजिक न्याय और आर्थिक समता आधारित कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। इनके जरिए राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह समाज में असमानताओं को कम करे, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करे, समानता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे, और सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई ऐसा हो पाया है?
सामाजिक असर की दृष्टि से, निर्देशक सिद्धांतों ने गरीबों, अल्पसंख्यकों, दलितों और कमजोर तबकों के लिए न्यायसंगत नीतियों के निर्माण को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, आरक्षण व्यवस्था, भूमि सुधार, और शिक्षा व रोजगार के अवसरों में समता जैसे कदम इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर लागू हुए। साथ ही, ये सिद्धांत सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और भेदभाव के विरुद्ध कानून बनाने में महत्वपूर्ण सहायक रहे हैं।
न्यायपालिका ने भी इन सिद्धांतों को सामाजिक बदलावों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार कर संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में (जैसे महिला समानता, निजता अधिकार, समलैंगिक संबंधों की वैधता) सामाजिक बदलावों को संवैधानिक निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर संवैधानिक न्याय का हिस्सा बनाया है, जिससे सामाजिक न्याय और अधिकारों की रक्षा हुई है।
हालांकि, ये सिद्धांत सीधे न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन इन्हें नीति निर्धारण और सामाजिक सुधारों के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। इन्हें लागू करने में चुनौतियां हैं, लेकिन इनके सामाजिक प्रभाव ने भारत को सामाजिक न्याय के रास्ते पर अग्रसरित किया है और समाज के कमजोर तबकों को सशक्त बनाया है। इस प्रकार, संवैधानिक निर्देशक सिद्धांतों ने भारतीय समाज में असमानता और अन्याय कम करने, सामाजिक समावेशन बढ़ाने, और मूलभूत मानवाधिकारों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक