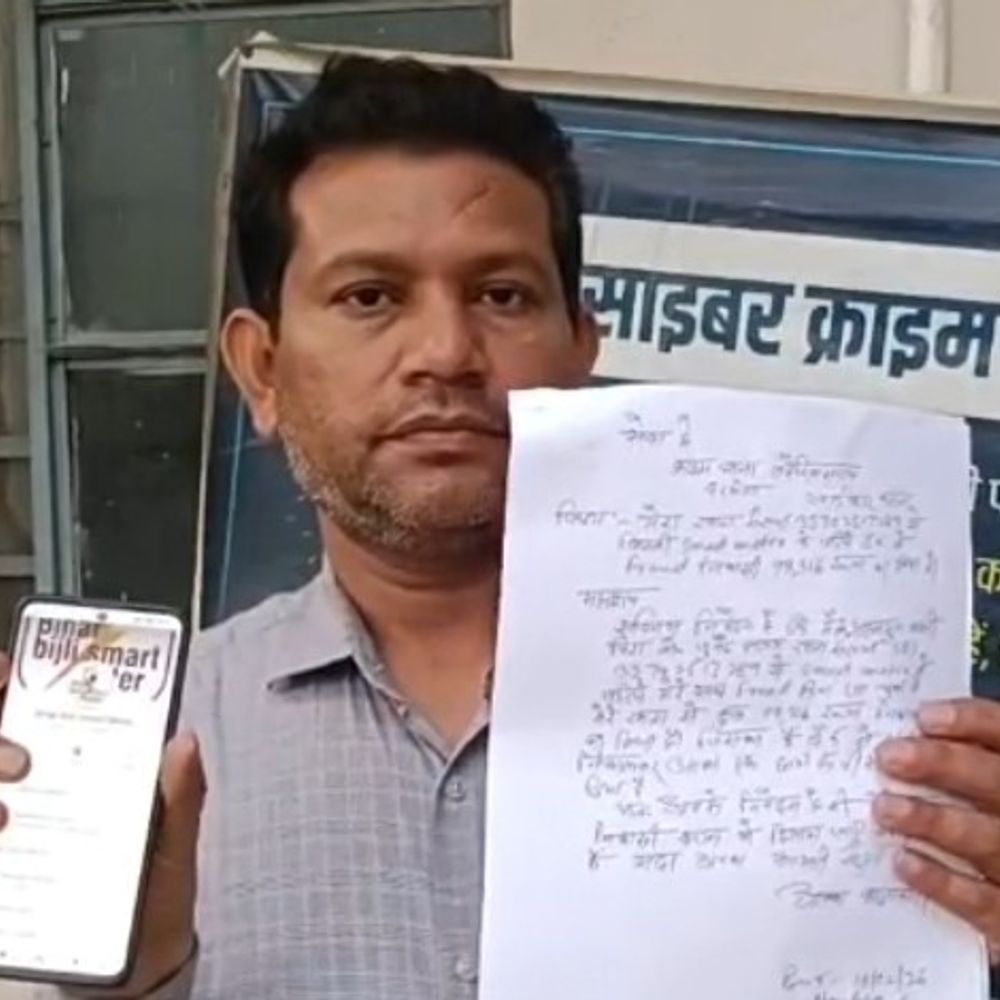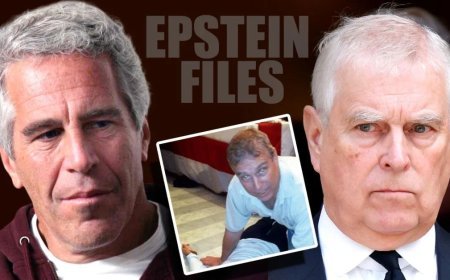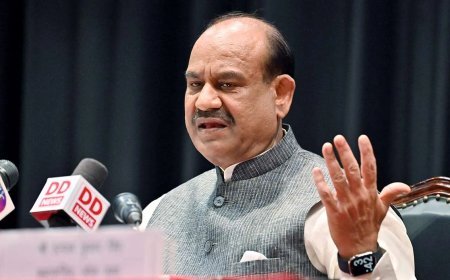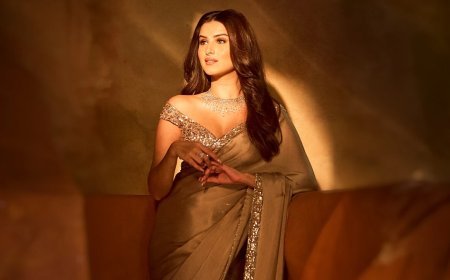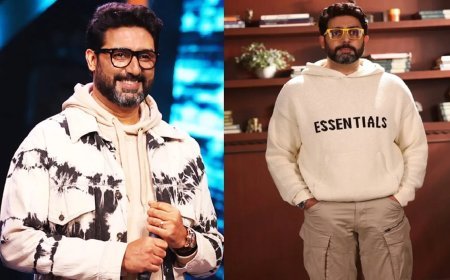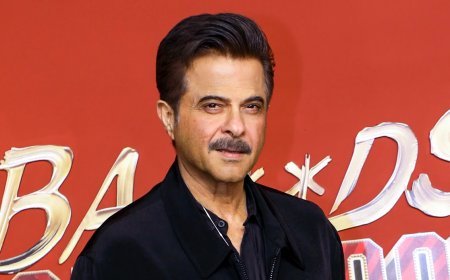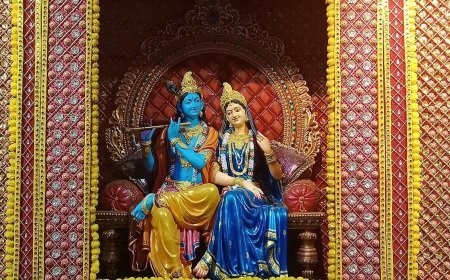भारतीय राजनीति में कांग्रेस (आई) एक मध्यम मार्गी पार्टी समझी जाती है, जो दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा से सर्वथा भिन्न प्रतीत होती आई है। लेकिन अभूतपूर्व बिहार विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसे 'मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस' (एमसीसी- बिहार का एक खूंखार नक्सली संगठन) कहना अनायास नहीं है, बल्कि उसके समकालीन सियासी विचलन पर एक करारा राजनीतिक प्रहार समझा जा रहा है।
देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस की इस दुःखती रग को दबाने के स्पष्ट सियासी मायने हैं, जिससे सबक लेकर जड़वत हो चली कांग्रेस अपना अहिल्या उद्धार कर सकती है। इससे कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न भी साकार नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की हार्दिक इच्छा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। वह पाकिस्तान के जनक 'मुस्लिम लीग' और बिहार की नक्सल संस्था माओवादी कोआर्डिनेशन कमेटी (एमसीसी) की ट्रू कॉपी बनने से परहेज करे। क्योंकि इससे देश विरोधी आतंकवादियों और नक्सलियों को बल मिलेगा।
ऐसे में सुलगता हुआ सवाल है कि 'बिटवीन द लाइन्स' से उसका विचलन या भटकाव कब और कैसे शुरू हुआ? इससे कांग्रेस पार्टी को लाभ मिला या घाटा हुआ! क्योंकि कांग्रेस का वैचारिक पतन भारतीय राजनीति के साथ-साथ खुद उसके अस्तित्व के लिए भी एक गम्भीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। नेहरू के वैश्विक सूझबूझ, इंदिरा की राष्ट्रीय पराक्रम और राजीव के टेक्नोक्रेटिक सौम्यता से जो पार्टी सिंचित हुई हो, उसपर ऐसा सियासी लांछन चिंता और चिंतन दोनों का विषय है।
ऐसा इसलिए कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, देश की लौह महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कतिपय राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, वैश्विक व क्षेत्रीय दर्शन की छाप परवर्ती बाजपेयी और मोदी सरकार पर भी कुछेक मायनों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यही उनकी नीतिगत प्रासंगिकता है जिसे कदापि झुठलाया नहीं जा सकता।
तीखा सवाल है कि एक विदेशी व्यक्ति 'ए ओ ह्यूम' द्वारा अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जनांकांक्षाओं के 'सेफ्टी वॉल्व' के रूप में स्थापित कांग्रेस पार्टी, आखिर में आजादी के बाद भी ब्रिटिशर्स की 'फूट डालो और शासन करो' वाली खतरनाक जातिवादी व सांप्रदायिक नीतियों की अनुगामी कब और कैसे बन गई? जबकि तल्ख सच्चाई है कि मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक आह्वान, वामपंथियों के वर्गवादी षड्यंत्र और समाजवादियों के जातीय आह्वान से कांग्रेस नेतृत्व को समय-समय पर न केवल दो-चार होना पड़ा, बल्कि गम्भीर सियासी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। इसी ऊहापोह में वह पतनोन्मुख भी हो गई।
अहम सवाल है कि राजनीति की आड़ में देश व समाज में सक्रिय सांप्रदायिक ताकतों, जातिवादी सूरमाओं, वर्गवादी षड्यंत्रकारियों, क्षेत्रवादियों की अनदेखी कांग्रेस ने क्यों की?
वहीं, अपराधियों, नक्सलियों व आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक मुहिम छेड़ते वक्त उसके रणनीतिकारों द्वारा भेदभाव क्यों किया गया? चाहे हिंदुओं के हिस्से वाले हिन्दुस्तान पर पंथनिरपेक्षता (धर्मनिरपेक्षता) थोपने की बात हो, या फिर समग्र व संतुलित विकास की जगह तुष्टीकरण की सियासत को शह देने की बात हो, क्या यह सब महज सियासी बहुमत की प्राप्ति के लिए किया गया, जो प्रवृत्ति आज देश व समाज के समक्ष एक नया नासूर प्रतीत हो रही है।
एक और अहम सवाल यह है कि विदेशी ताकतों के समक्ष घुटने क्यों टेके गए? रोटी, कपड़ा और मकान के नारे तो दिए गए, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य व सम्मान की बात क्यों दरकिनार कर दी गई। कोढ़ में खाज यह कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक नहीं बल्कि दो-तीन बार प्रतिबंध तो लगाया गया? लेकिन मुस्लिम लीग के क्लोन बन चुके अतिवादी संगठनों को ढील क्यों दी गई। सिख आतंकवादियों के खिलाफ जितनी सख्ती दिखाई गई, वैसी ही सख्ती मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ क्यों नहीं दिखाई गई?
यही नहीं, ब्रेक के बाद होने वाले सांप्रदायिक दंगों और जातीय संघर्षों के खिलाफ कड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए? कानूनी विसंगतियों को दूर करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। ऐसे बहुत से सवाल हैं, जिनका उत्तर हर प्रबुद्ध भारतीय चाहेगा, क्योंकि इन्हीं से जुड़े अदूरदर्शिता भरे टालमटोल वाले निर्णयों में कांग्रेस के लगातार कमजोर होते जाने के संकेत छिपे हैं। हद तो यह कि जिन वामपंथियों, समाजवादियों ने कांग्रेस को कमजोर किया, फिर उन्हीं के साथ गठबंधन करके अपना बचा-खुचा जनाधार क्यों सौंप दिया गया?
इस प्रकार भारतीय राजनीति में कांग्रेस के पतन के सियासी प्रभाव को व्यापक और दूरगामी बताया जा रहा है, जिसमें नेतृत्व की कमजोरी, आंतरिक कलह, गठबंधन अस्थिरता, क्षेत्रीय दलों के उभार और भाजपा के सशक्त संगठन का बड़ा योगदान है। मेरे विचार से कांग्रेस के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-
पहला, पार्टी के नेतृत्व का संकट: कांग्रेस में लंबे समय से स्पष्ट और प्रभावशाली नेतृत्व की कमी देखी गई है। चाहे पंडित जवाहर लाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, या राजीव गांधी हों, सबने प्रतिभाशाली नेताओं को दरकिनार किया और चापलूसों को बढ़ावा दिया। सूबाई नेतृत्व को कभी भी जमने का मौका नहीं दिया। बार बार राज्यों के मुख्यमंत्री बदले गए। इनके बाद वाले शीर्ष नेताओं यथा- सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने असहमति से निबटने और पार्टी के भीतर गुटबाजी के लगातार बढ़ने को थामने का कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं किया। खैर, सोनिया गांधी ने तो कुछ समझदारी भी दिखाई, लेकिन राहुल गांधी-प्रियंका गांधी अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगातार विफल साबित हुए हैं। इसलिए उन्हें खुद आत्ममंथन करना चाहिए।
दूसरा, पार्टी के नेताओं की आंतरिक कलह: कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के असंतोष और पार्टी छोड़ने जैसी घटनाएँ निरंतर पार्टी की आधार को कमजोर करती रही हैं। अपनी स्थापना के 4-5 दशक बाद ही पार्टी गम्भीर मतभेदों की शिकार हो गई। महात्मा गांधी का पक्षधर मिजाज, नेहरू जी की स्वार्थपरकता, इंदिरा जी की हठधर्मिता और राजीव गांधी की सियासी अनुभवहीनता से बहुत सारे गलत निर्णय हुए, जो देर सबेर कांग्रेस व उसके विभिन्न स्तरीय नेतृत्व पर भारी पड़े। वैसे भी संगठन विस्तार और विचारधारा के स्तर पर मतभेद अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन उनपर पारदर्शी बहस की हमेशा कमी महसूस हुई। यही वजह है कि कांग्रेस कई बार टूटी भी, लेकिन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने उनका बखूबी मुकाबला किया और खुद को मुख्यधारा वाली कांग्रेस साबित किया। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने पुराने नेताओं को पार्टी से जोड़े रखने में विफल रहे। जबकि उन्हें चाहिए कि वह पुराने, उम्रदराज और वफादार नेताओं का मानमनौव्वल करके भी पार्टी से उन्हें जोड़े रखें। अपनी पार्टी के अनुभवी सहयोगियों को भी पार्टी से जोड़े रखें, जबकि वे सबको रोकने में विफल रहे। इससे नेतृत्व संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं, युवा नेतृत्व भी नहीं पनप पा रहा है। यह कांग्रेस का सबसे बड़ा रणनीतिक संकट है।
तीसरा, कांग्रेस के वोट बैंक पर क्षेत्रीय दलों का उभार: सूबाई राजनीति में पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आंध्रप्रदेश की वाईएसआरकांग्रेस आदि तो कांग्रेस से निकली और सफल रही पार्टियां हैं। वहीं, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के दलित-अल्पसंख्यक जनाधार को हसोथ लिया है। आम आदमी पार्टी, डीएमके, बीजेडी, नेशनल कांफ्रेंस, बसपा, लोजपा आदि से गठबंधन करके कांग्रेस ने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। इंडिया गठबंधन के नाम पर एकजुट हुए दल भी कांग्रेस के वोट से ही जनाधार वाले बने और कांग्रेस की ही नुक्ताचीनी शुरू कर दी, जिसकी सियासी कीमत कांग्रेस ने महाराष्ट्र, हरियाणा व दिल्ली विधानसभा चुनावों में चुकाई। विचारणीय सवाल है कि इन जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन देने से बेहतर है कि उनके इलाके में कांग्रेस के स्वाभाविक नेतृत्व को विकसित होने दिया जाये, ताकि कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में कोई दूसरा सेंध नहीं लगा सके। राज्यों में कांग्रेस का असर उसके सहयोगियों के चलते ही घटता जा रहा है, क्योंकि वे कांग्रेस को परजीवी बनाना चाहते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तरप्रदेश में अखिलेश यादव के सियासी व्यवहार से कांग्रेस नेतृत्व को समय रहते ही सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये राहुल-प्रियंका के सहयोगी नहीं, बल्कि मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरेंगे, जब पीएम बनने की बारी आएगी।
चौथा, कमजोर संगठनात्मक ढाँचा: जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन अब उतना प्रभावशाली नहीं है, जितना वह पहले था। खासकर सेवा दल, युवा कांग्रेस आदि का प्रभाव अब बेहद कम हुआ है, अन्यथा पहले इनकी तूती बोलती थी। इसके पीछे पार्टी नेतृत्व और उनके चाटूकार नेताओं द्वारा जमीनी सशक्त नेतृत्व की सियासी भ्रूणहत्या की नापाक कोशिशें रही हैं। आज पंचायत स्तर पर, शहरी वार्ड स्तर पर, प्रखंड और जिला स्तर पर स्वाभाविक नेतृत्व को कभी पनपने ही नहीं दिया गया। कुछ धन्नासेठों व पुराने राजनीतिक परिवारों के लगुवे-भगुवे को संगठनात्मक पद या टिकट देने की जो प्रवृत्ति पार्टी में घर कर गई है, उससे पार्टी का जनाधार खिसका है। चूंकि प्रदेश स्तर पर नेतृत्व में स्थायित्व नहीं है, इसलिए जिला व प्रखंड स्तर पर पार्टी निरंतर कमजोर होती जा रही है। जनहित के मुद्दों से उसका वास्ता ऑन द स्पॉट नहीं है, बल्कि मीडिया व सोशल मीडिया तक सीमित है। धरना-प्रदर्शन भी सिर्फ खानापूर्ति भर के लिए किए जाते हैं।
पांचवां, पार्टी की नीतिगत अस्पष्टता: पहले कांग्रेस एक नीतिगत पार्टी थी, जिससे भारतीयता की झलक मिलती थी। यह मध्यममार्गी पार्टी इसलिए समझी जाती थी कि इसने विचारधारा के स्तर पर सदैव मध्यम मार्ग यानी सबका भला सोचने को प्राथमिकता दी। इसने उग्र वामपंथ और दक्षिणपंथ को कभी प्रश्रय नहीं दिया। यह पूँजीवाद और साम्यवाद से इतर नागरिक समाजवाद पर जोर देती रही और मिश्रित अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जिससे सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों ने आशातीत उन्नति की। लेकिन बाद के वर्षों में पार्टी के नीतिगत एजेंडे में व्यापक बदलाव आया। वह सांप्रदायिक व जातिवादी ताकतों के समक्ष घुटने टेकने लगी। क्षेत्रवादियों, नक्सलियों, आतंकवादियों, संगठित अपराधियों, भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को कुचलने के बजाए, वह उनसे क्षणिक समझौते करने लगी। इससे पार्टी के आलोचक बढ़े और तुष्टीकरण के आरोप मढ़ने लगे। यही बात पार्टी पर भारी पड़ी। वहीं, इस ओर से मुखर युवाओं और मध्यम वर्ग को जोड़ पाने में कांग्रेस पूरी तरह से असफलता रही है। इस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति और अहम मुद्दों पर कथनी-करनी में अंतर ने भी कांग्रेस को भारी नुकसान पहुँचाया।
कांग्रेस की उपर्युक्त नीतिगत लापरवाही का सियासी असर और परिणाम यह हुआ कि भाजपा का वर्चस्व लगातार बढ़ता चला गया। पहले भाजपा ने समाजवादियों, फिर दलितवादियों से समझौते किए, जिससे कांग्रेस को कमजोर करने में वह सफल रही। चूंकि कांग्रेस के कमजोर होने का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिला है, जिसने अवसर का लाभ उठाकर राष्ट्रीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। भाजपा ने भी समय के साथ धर्मनिरपेक्ष समाजवादियों-दलितवादियों को ठेंगा दिखाया और गठबंधन की राजनीति करके राज्यीय और राष्ट्रीय राजनीति में काफी मजबूत हो गई। मंडल और कमंडल की राजनीति उसके मध्यम मार्ग पर इतनी भारी पड़ी कि राज्यों में मण्डलवादियों ने और केंद्र में कमण्डलवादियों ने अपना वर्चस्व जमा लिया। फिर दोनों का घालमेल करके कांग्रेस व उसके समर्थकों को भी अप्रासंगिक बना दिया। इसलिए मेरी निजी राय है कि कांग्रेस खुद को जातिवादी और सम्प्रदायवादी सियासत से दूर रखे। वह रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान की राजनीति करे। भावनात्मक राजनीति से दूरी बनाए। मूल मुद्दों पर होमवर्क करे और फिर सही समय का इंतजार करे।
कांग्रेस की कमजोरी से गठबंधन राजनीति की नई मजबूरी पैदा हो गई। आलम यह है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर शासन के लिए अक्सर क्षेत्रीय दलों से गठजोड़ करना पड़ता है, जो अक्सर अस्थिर साबित होते हैं। ऐसा करने से कांग्रेस के प्रोग्रेसिव एजेंडे में भी कमी आती है। लिहाजा, कांग्रेस की सकारात्मक और प्रगतिशील नीति का अभाव इसे सत्ताधारी विकल्प के रूप में कमजोर बना देता है। परिणाम यह होता है कि उसका वोट बैंक बिखर जाता है। यह कड़वा सच है कि पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक यथा- सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक, अब विभाजित होकर अन्य पार्टियों की तरफ चला गया है, जिससे चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। उसके समक्ष अब भविष्य की चुनौती समुपस्थित है। इसलिए नेतृत्व में स्थिरता लाना, संगठन को मजबूत बनाना, युवा और नए वर्गों को साथ जोड़ना और स्पष्ट नीति साधना कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक है। वहीं, क्षेत्रीय दलों से प्रतिस्पर्धा तथा भाजपा के संगठनात्मक स्तर का मुकाबला करना भी बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर, कांग्रेस के पतन का सियासी असर भारत की राजनीति को बहुदलीय और प्रतिस्पर्धात्मक बना देता है, जिससे सत्ता तथा नीति निर्धारण के स्तर पर निरंतर बदलाव आते हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस इससे सबक लेगी।
- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक