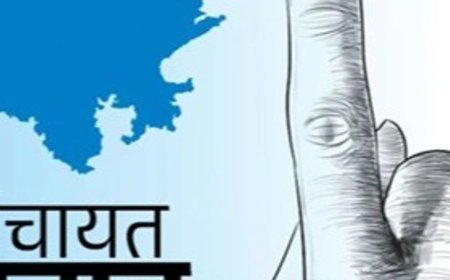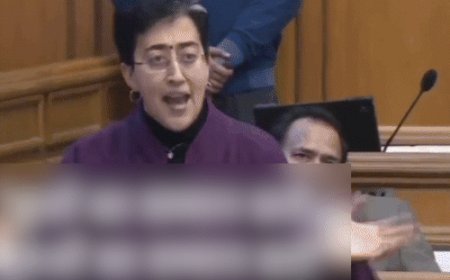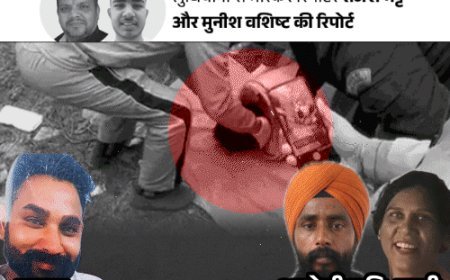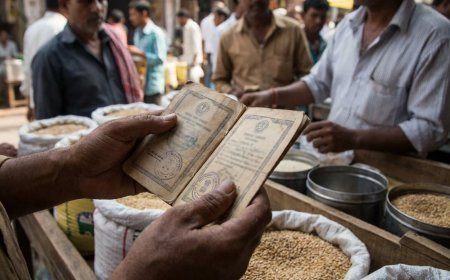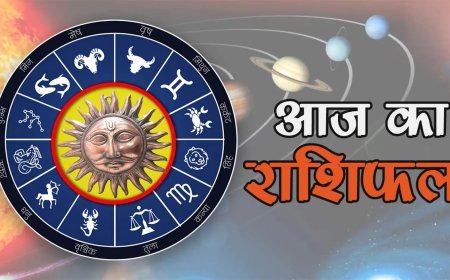इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तीन दिनों से जारी शांति वार्ता सोमवार को बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गई। तुर्की की मेज़बानी और कतर की मध्यस्थता में हुई इन वार्ताओं का उद्देश्य सीमा पर बढ़ते संघर्षों को रोकना और 19 अक्टूबर को हुए युद्धविराम को स्थायी रूप देना था। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने सीमा पार से हो रहे हमलों, आतंकवादी गतिविधियों और पारस्परिक आरोपों पर चर्चा की, परंतु कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हुआ। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अफगान प्रतिनिधिमंडल बार-बार काबुल से परामर्श ले रहा था और पाकिस्तान को “प्रोत्साहनहीन” जवाब मिल रहा था।
इस बीच, पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि वार्ता के दौरान ही सीमा पर दो बड़े घुसपैठ प्रयासों को नाकाम करते हुए 25 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि पाँच पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी।
उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मलेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि वह इस संकट को “बहुत जल्द” सुलझा लेंगे। उन्होंने इस्लामाबाद और काबुल के बीच शांति प्रयासों का स्वागत किया और कहा कि दोनों देशों को “स्थायी समाधान” की दिशा में बढ़ना चाहिए।
हम आपको बता दें कि तुर्की और क़तर के अधिकारी, जिन्होंने इन वार्ताओं की मेज़बानी की, अब यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि संवाद पूरी तरह विफल नहीं हो। पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने अफगान पक्ष से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के खिलाफ “ठोस और सत्यापन योग्य कार्रवाई” की मांग की है।
देखा जाये तो इस्तांबुल में हुई यह वार्ता केवल दो देशों के बीच बातचीत नहीं थी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता की परीक्षा थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान— दोनों ऐसे देश हैं जहाँ दशकों से अस्थिरता, आतंकवाद और सीमा विवादों ने राजनीतिक ढांचे को जकड़ रखा है। तालिबान की सत्ता में वापसी (2021) के बाद पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि काबुल की नई सरकार उसके प्रति अधिक सहानुभूति रखेगी और सीमा-पार आतंकवाद पर लगाम लगाएगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत हुआ। अफगान धरती से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने हमले बढ़ा दिए और पाकिस्तान की पश्चिमी सीमाएँ फिर से असुरक्षित हो गईं।
इस वार्ता के दौरान पाकिस्तान की मांगें स्पष्ट थीं— अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान-विरोधी आतंकवाद के लिए नहीं होने दे। दूसरी ओर, अफगान तालिबान का रुख यह था कि पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण में सुधार करे। दरअसल यह संवाद इसलिए अटक गया क्योंकि दोनों पक्षों में “विश्वास की कमी” की खाई गहरी है।
हम आपको यह भी बता दें कि तुर्की और कतर इस पूरी प्रक्रिया के मध्यस्थ मात्र नहीं, बल्कि इस्लामी विश्व की नई कूटनीतिक धुरी बनकर उभरे हैं। दोनों देश यह दिखाना चाहते हैं कि पश्चिमी मध्यस्थता के बिना भी मुस्लिम विश्व अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझा सकता है। परंतु यह प्रयास तब तक सफल नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने भू-राजनीतिक एजेंडे से ऊपर उठकर आपसी भरोसे का पुल नहीं बनाते।
उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान से स्पष्ट है कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, बल्कि “प्रेरक” की भूमिका निभा रहा है। यह स्थिति भारत के लिए मिश्रित प्रभाव रखती है— एक ओर अमेरिका की दूरी भारत के रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का अवसर देती है, दूसरी ओर चीन और रूस जैसे देशों के लिए क्षेत्रीय हस्तक्षेप का दरवाजा खोलती है। देखा जाये तो भारत के दृष्टिकोण से यह वार्ता केवल एक पड़ोसी संघर्ष नहीं, बल्कि एक सामरिक परिदृश्य है जिसके परिणाम गहरे हो सकते हैं।
यदि पाकिस्तान अपने पश्चिमी मोर्चे पर उलझा रहता है, तो उसकी पूर्वी सीमा यानी भारत के साथ वाली सीमा पर दबाव अपेक्षाकृत कम होगा। लेकिन इतिहास बताता है कि जब भी पाकिस्तान आंतरिक संकट में घिरता है, वह ध्यान भटकाने के लिए भारत-विरोधी गतिविधियों को तेज़ करता है।
भारत ने पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान में स्कूलों, सड़कों और संसद भवन जैसी परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। यदि काबुल में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, तो भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ को नुकसान होगा और मध्य एशिया तक पहुँच का सपना बाधित हो सकता है।
वहीं चीन पहले से ही चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के माध्यम से क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा रहा है। अब वह अफगानिस्तान में भी निवेश बढ़ा रहा है। यदि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का त्रिकोण सशक्त होता है, तो भारत को उत्तरी सीमाओं से लेकर हिंद महासागर तक नए सुरक्षा समीकरणों से जूझना पड़ेगा।
दूसरी ओर, टीटीपी, इस्लामिक स्टेट-खुरासान (IS-K) जैसे गुटों की गतिविधियाँ यदि अफगानिस्तान से नियंत्रित नहीं हुईं, तो इसका असर कश्मीर और भारतीय उपमहाद्वीप की सुरक्षा नीति पर भी पड़ेगा। इसलिए भारत को अपने खुफिया सहयोग और सीमा निगरानी को और सशक्त करना होगा।
देखा जाये तो इस्तांबुल की वार्ता का निष्कर्षहीन रहना यह दर्शाता है कि दक्षिण एशिया अभी भी पुराने अविश्वासों के घेरे से मुक्त नहीं हो पाया है। पाकिस्तान-अफगान सीमा, जो कभी अमेरिकी “वार ऑन टेरर” का केंद्र रही, आज भी बारूद के ढेर पर बैठी है। भारत के लिए इस स्थिति में संतुलित लेकिन सतर्क नीति आवश्यक है— न तो भावनात्मक प्रतिक्रिया, न ही उदासीन दूरी। भारत को चाहिए कि वह अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों पर “स्थायी शांति” के विचार को आगे बढ़ाए, साथ ही अपनी सामरिक तैयारी और खुफिया दक्षता को और मज़बूत रखे।
इस्तांबुल संवाद यह याद दिलाता है कि शांति केवल कूटनीति से नहीं आती; उसके लिए ईमानदारी, विश्वास और दीर्घकालिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब तक काबुल और इस्लामाबाद अपनी ऐतिहासिक असुरक्षाओं से मुक्त नहीं होते, तब तक यह क्षेत्र शांति के बजाय अस्थिरता के चक्र में फँसा रहेगा और भारत को इसके हर पड़ाव के लिए तैयार रहना होगा। कुल मिलाकर देखें तो यह वार्ता असफल नहीं, बल्कि एक “परीक्षण का दौर” है जहाँ दक्षिण एशिया की नियति तय हो रही है। सवाल यह नहीं कि इस्तांबुल में क्या हुआ, बल्कि सवाल यह है कि क्या इस क्षेत्र के देश शांति की राह पर चलने का साहस जुटा पाएँगे?
भारत को इस प्रश्न का उत्तर देने में निर्णायक भूमिका निभानी होगी।